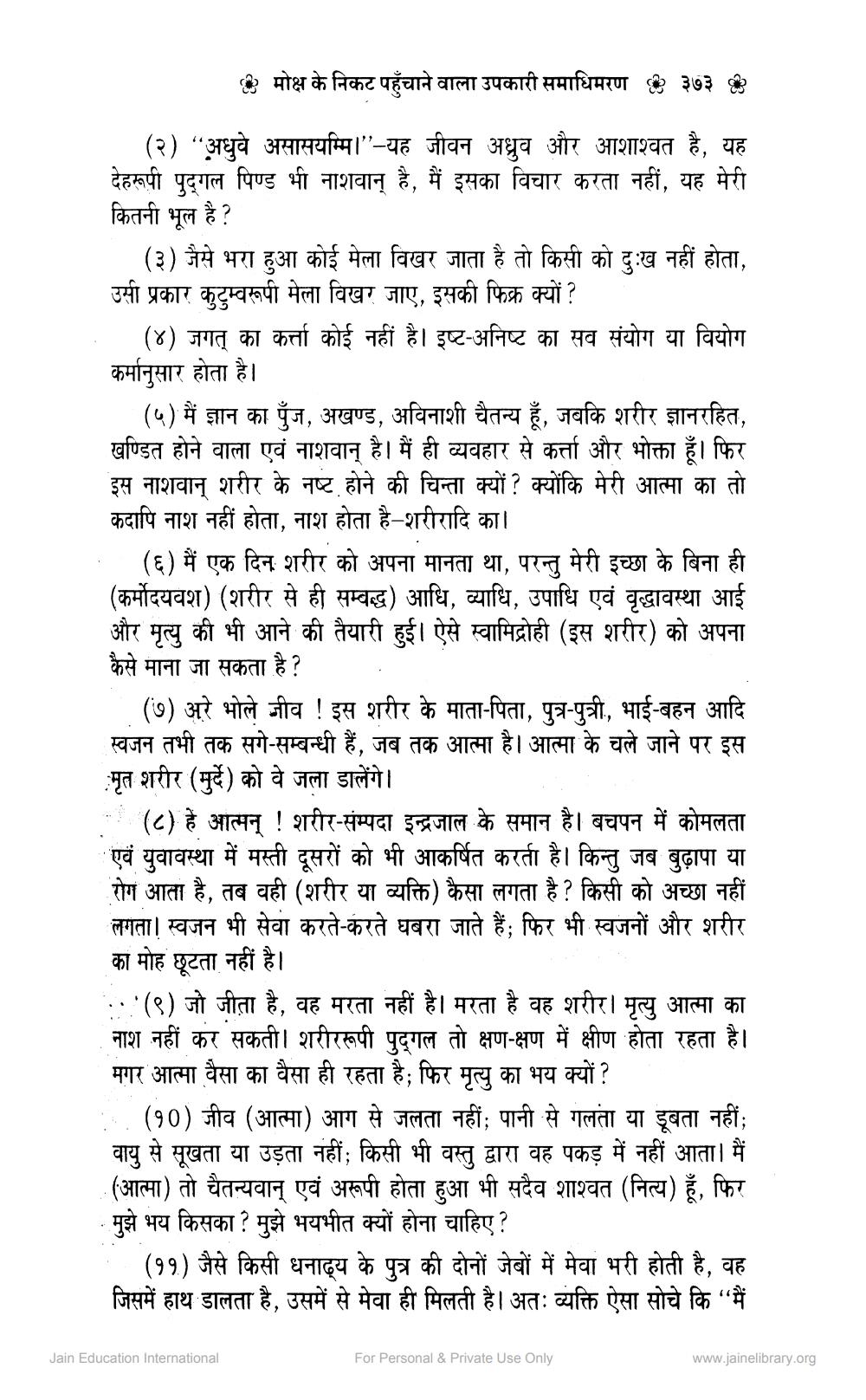________________
0 मोक्ष के निकट पहुँचाने वाला उपकारी समाधिमरण 8 ३७३ 2
(२) "अधुवे असासयम्मि।'' यह जीवन अध्रुव और आशाश्वत है, यह देहरूपी पुद्गल पिण्ड भी नाशवान् है, मैं इसका विचार करता नहीं, यह मेरी कितनी भूल है?
(३) जैसे भरा हुआ कोई मेला विखर जाता है तो किसी को दुःख नहीं होता, उसी प्रकार कुटुम्वरूपी मेला विखर जाए, इसकी फिक्र क्यों ?
(४) जगत् का कर्ता कोई नहीं है। इष्ट-अनिष्ट का सव संयोग या वियोग कर्मानुसार होता है।
(५) मैं ज्ञान का पुँज, अखण्ड, अविनाशी चैतन्य हैं, जबकि शरीर ज्ञानरहित. खण्डित होने वाला एवं नाशवान् है। मैं ही व्यवहार से कर्ता और भोक्ता हूँ। फिर इस नाशवान् शरीर के नष्ट होने की चिन्ता क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा का तो कदापि नाश नहीं होता, नाश होता है-शरीरादि का।
(६) मैं एक दिन शरीर को अपना मानता था, परन्तु मेरी इच्छा के बिना ही (कर्मोदयवश) (शरीर से ही सम्बद्ध) आधि, व्याधि, उपाधि एवं वृद्धावस्था आई
और मृत्यु की भी आने की तैयारी हुई। ऐसे स्वामिद्रोही (इस शरीर) को अपना कैसे माना जा सकता है?
(७) अरे भोले जीव ! इस शरीर के माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन आदि स्वजन तभी तक सगे-सम्बन्धी हैं, जब तक आत्मा है। आत्मा के चले जाने पर इस मृत शरीर (मुर्दे) को वे जला डालेंगे।
(८) हे आत्मन् ! शरीर-संम्पदा इन्द्रजाल के समान है। बचपन में कोमलता एवं युवावस्था में मस्ती दूसरों को भी आकर्षित करती है। किन्तु जब बुढ़ापा या रोग आता है, तब वही (शरीर या व्यक्ति) कैसा लगता है ? किसी को अच्छा नहीं लगता। स्वजन भी सेवा करते-करते घबरा जाते हैं; फिर भी स्वजनों और शरीर का मोह छूटता नहीं है। . . . (९) जो जीता है, वह मरता नहीं है। मरता है वह शरीर। मृत्यु आत्मा का नाश नहीं कर सकती। शरीररूपी पुद्गल तो क्षण-क्षण में क्षीण होता रहता है। मगर आत्मा वैसा का वैसा ही रहता है; फिर मृत्यु का भय क्यों? ... (१०) जीव (आत्मा) आग से जलता नहीं; पानी से गलता या डूबता नहीं; वायु से सूखता या उड़ता नहीं; किसी भी वस्तु द्वारा वह पकड़ में नहीं आता। मैं (आत्मा) तो चैतन्यवान् एवं अरूपी होता हुआ भी सदैव शाश्वत (नित्य) हूँ, फिर मुझे भय किसका? मुझे भयभीत क्यों होना चाहिए?
(११) जैसे किसी धनाढ्य के पुत्र की दोनों जेबों में मेवा भरी होती है, वह जिसमें हाथ डालता है, उसमें से मेवा ही मिलती है। अतः व्यक्ति ऐसा सोचे कि “मैं
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org