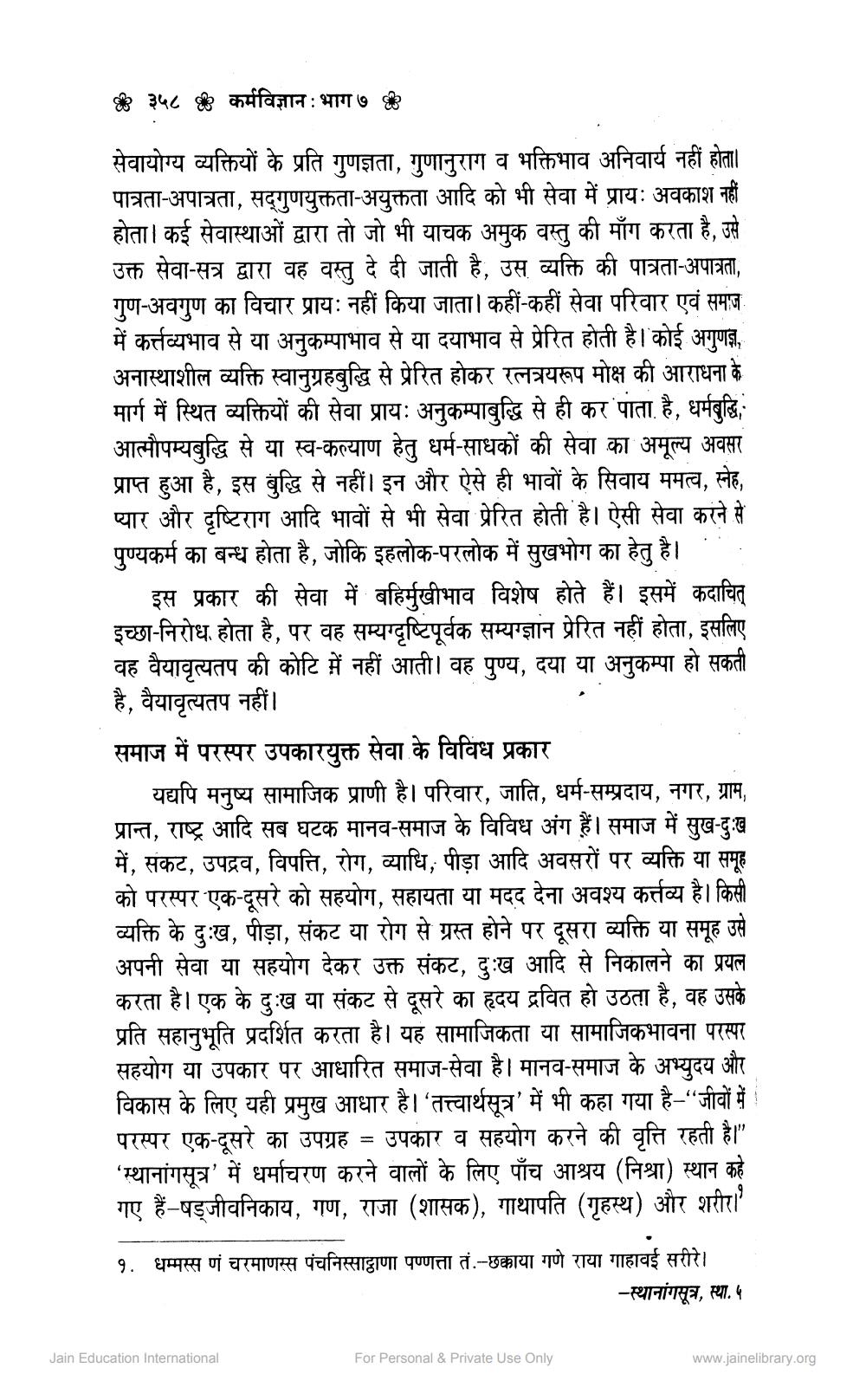________________
* ३५८ ॐ कर्मविज्ञान : भाग ७ *
सेवायोग्य व्यक्तियों के प्रति गुणज्ञता, गुणानुराग व भक्तिभाव अनिवार्य नहीं होता। पात्रता-अपात्रता, सद्गुणयुक्तता-अयुक्तता आदि को भी सेवा में प्रायः अवकाश नहीं होता। कई सेवास्थाओं द्वारा तो जो भी याचक अमुक वस्तु की माँग करता है, उसे उक्त सेवा-सत्र द्वारा वह वस्तु दे दी जाती है, उस व्यक्ति की पात्रता-अपात्रता, गुण-अवगुण का विचार प्रायः नहीं किया जाता। कहीं-कहीं सेवा परिवार एवं समाज में कर्तव्यभाव से या अनुकम्पाभाव से या दयाभाव से प्रेरित होती है। कोई अगुणज्ञ, अनास्थाशील व्यक्ति स्वानुग्रहबुद्धि से प्रेरित होकर रत्नत्रयरूप मोक्ष की आराधना के मार्ग में स्थित व्यक्तियों की सेवा प्रायः अनुकम्पाबुद्धि से ही कर पाता है, धर्मबुद्धि, आत्मौपम्यबुद्धि से या स्व-कल्याण हेतु धर्म-साधकों की सेवा का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है, इस बुद्धि से नहीं। इन और ऐसे ही भावों के सिवाय ममत्व, स्नेह, प्यार और दृष्टिराग आदि भावों से भी सेवा प्रेरित होती है। ऐसी सेवा करने से पुण्यकर्म का बन्ध होता है, जोकि इहलोक-परलोक में सुखभोग का हेतु है।
इस प्रकार की सेवा में बहिर्मुखीभाव विशेष होते हैं। इसमें कदाचित् इच्छा-निरोध होता है, पर वह सम्यग्दृष्टिपूर्वक सम्यग्ज्ञान प्रेरित नहीं होता, इसलिए वह वैयावृत्यतप की कोटि में नहीं आती। वह पुण्य, दया या अनुकम्पा हो सकती है, वैयावृत्यतप नहीं। समाज में परस्पर उपकारयुक्त सेवा के विविध प्रकार
यद्यपि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परिवार, जाति, धर्म-सम्प्रदाय, नगर, ग्राम, प्रान्त, राष्ट्र आदि सब घटक मानव-समाज के विविध अंग हैं। समाज में सुख-दुःख में, संकट, उपद्रव, विपत्ति, रोग, व्याधि, पीड़ा आदि अवसरों पर व्यक्ति या समूह को परस्पर एक-दूसरे को सहयोग, सहायता या मदद देना अवश्य कर्तव्य है। किसी व्यक्ति के दुःख, पीड़ा, संकट या रोग से ग्रस्त होने पर दूसरा व्यक्ति या समूह उसे अपनी सेवा या सहयोग देकर उक्त संकट, दुःख आदि से निकालने का प्रयल करता है। एक के दुःख या संकट से दूसरे का हृदय द्रवित हो उठता है, वह उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है। यह सामाजिकता या सामाजिकभावना परस्पर सहयोग या उपकार पर आधारित समाज-सेवा है। मानव-समाज के अभ्युदय और विकास के लिए यही प्रमुख आधार है। 'तत्त्वार्थसूत्र' में भी कहा गया है-“जीवों में परस्पर एक-दूसरे का उपग्रह = उपकार व सहयोग करने की वृत्ति रहती है।" 'स्थानांगसूत्र' में धर्माचरण करने वालों के लिए पाँच आश्रय (निश्रा) स्थान कहे गए हैं-षड्जीवनिकाय, गण, राजा (शासक), गाथापति (गृहस्थ) और शरीर।'
१. धम्मस्स णं चरमाणस्स पंचनिस्साट्ठाणा पण्णत्ता तं.-छक्काया गणे राया गाहावई सरीरे।
-स्थानांगसूत्र, स्था.५
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org