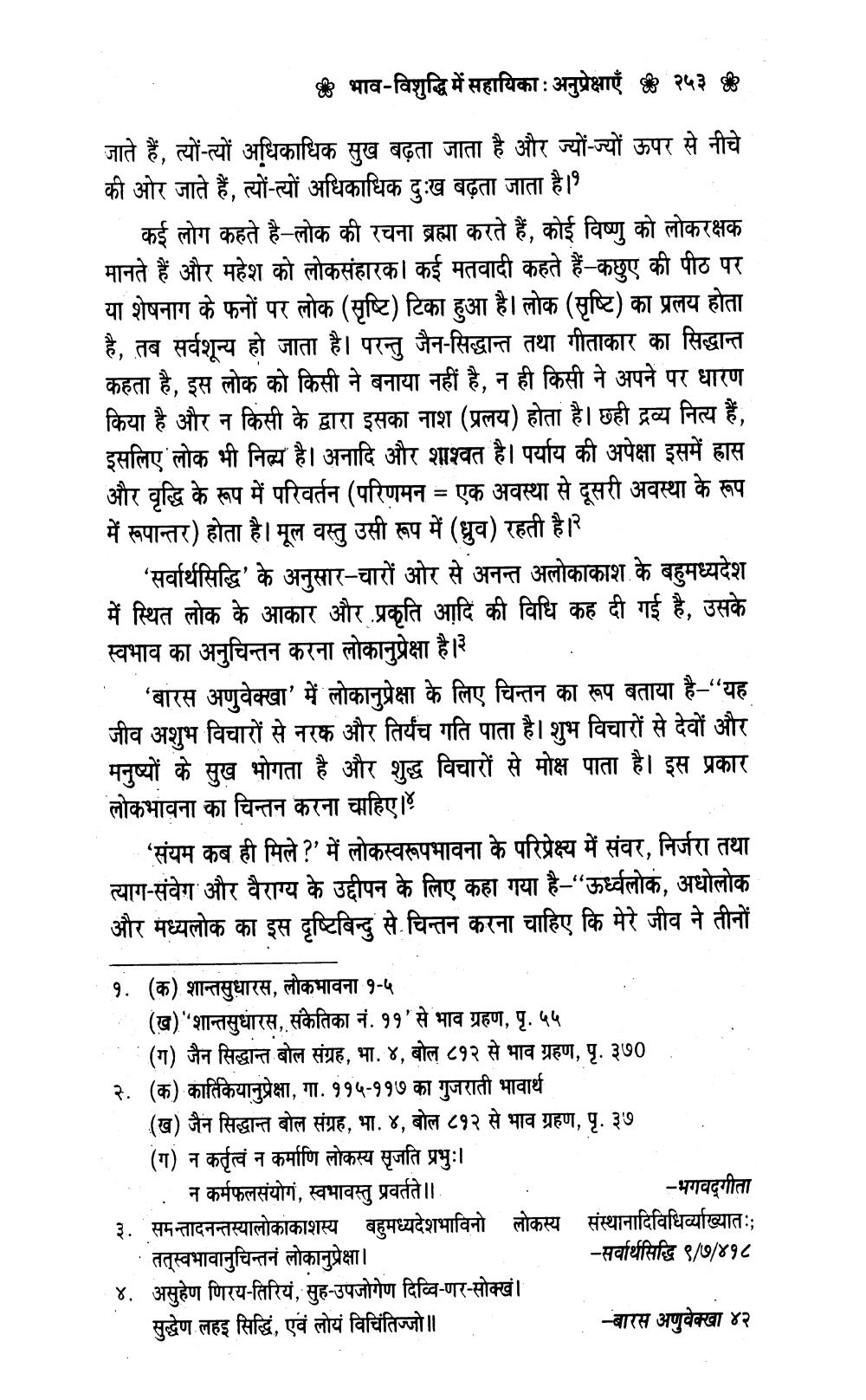________________
ॐ भाव-विशुद्धि में सहायिका : अनुप्रेक्षाएँ - २५३ ॐ
जाते हैं, त्यों-त्यों अधिकाधिक सुख बढ़ता जाता है और ज्यों-ज्यों ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, त्यों-त्यों अधिकाधिक दुःख बढ़ता जाता है।' ____ कई लोग कहते है-लोक की रचना ब्रह्मा करते हैं, कोई विष्णु को लोकरक्षक मानते हैं और महेश को लोकसंहारक। कई मतवादी कहते हैं-कछुए की पीठ पर या शेषनाग के फनों पर लोक (सृष्टि) टिका हुआ है। लोक (सृष्टि) का प्रलय होता है, तब सर्वशून्य हो जाता है। परन्तु जैन-सिद्धान्त तथा गीताकार का सिद्धान्त कहता है, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, न ही किसी ने अपने पर धारण किया है और न किसी के द्वारा इसका नाश (प्रलय) होता है। छही द्रव्य नित्य हैं, इसलिए लोक भी नित्य है। अनादि और शाश्वत है। पर्याय की अपेक्षा इसमें ह्रास
और वृद्धि के रूप में परिवर्तन (परिणमन = एक अवस्था से दूसरी अवस्था के रूप में रूपान्तर) होता है। मूल वस्तु उसी रूप में (ध्रुव) रहती है।२ ।। _ 'सर्वार्थसिद्धि' के अनुसार-चारों ओर से अनन्त अलोकाकाश के बहुमध्यदेश में स्थित लोक के आकार और प्रकृति आदि की विधि कह दी गई है, उसके स्वभाव का अनुचिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा है।३ ___ 'बारस अणुवेक्खा' में लोकानुप्रेक्षा के लिए चिन्तन का रूप बताया है-“यह जीव अशुभ विचारों से नरक और तिर्यंच गति पाता है। शुभ विचारों से देवों और मनुष्यों के सुख भोगता है और शुद्ध विचारों से मोक्ष पाता है। इस प्रकार लोकभावना का चिन्तन करना चाहिए।
- 'संयम कब ही मिले?' में लोकस्वरूपभावना के परिप्रेक्ष्य में संवर, निर्जरा तथा त्याग-संवेग और वैराग्य के उद्दीपन के लिए कहा गया है-“ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का इस दृष्टिबिन्दु से चिन्तन करना चाहिए कि मेरे जीव ने तीनों
१. (क) शान्तसुधारस, लोकभावना १-५
(ख) शान्तसुधारस, संकेतिका नं. ११' से भाव ग्रहण, पृ. ५५
(ग) जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, भा. ४, बोल ८१२ से भाव ग्रहण, पृ. ३७० २. (क) कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा. ११५-११७ का गुजराती भावार्थ
(ख) जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, भा. ४, बोल ८१२ से भाव ग्रहण, पृ. ३७ (ग) न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। . न कर्मफलसंयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते।
-भगवद्गीता ३. समन्तादनन्तस्यालोकाकाशस्य बहुमध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिळख्यातः; · तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेक्षा।
-सर्वार्थसिद्धि ९/७/४१८ ४. असुहेण णिरय-तिरियं, सुह-उपजोगेण दिग्वि-णर-सोक्खं । सुद्धण लहइ सिद्धिं, एवं लोयं विचिंतिज्जो॥
-बारस अणुवेस्खा ४२