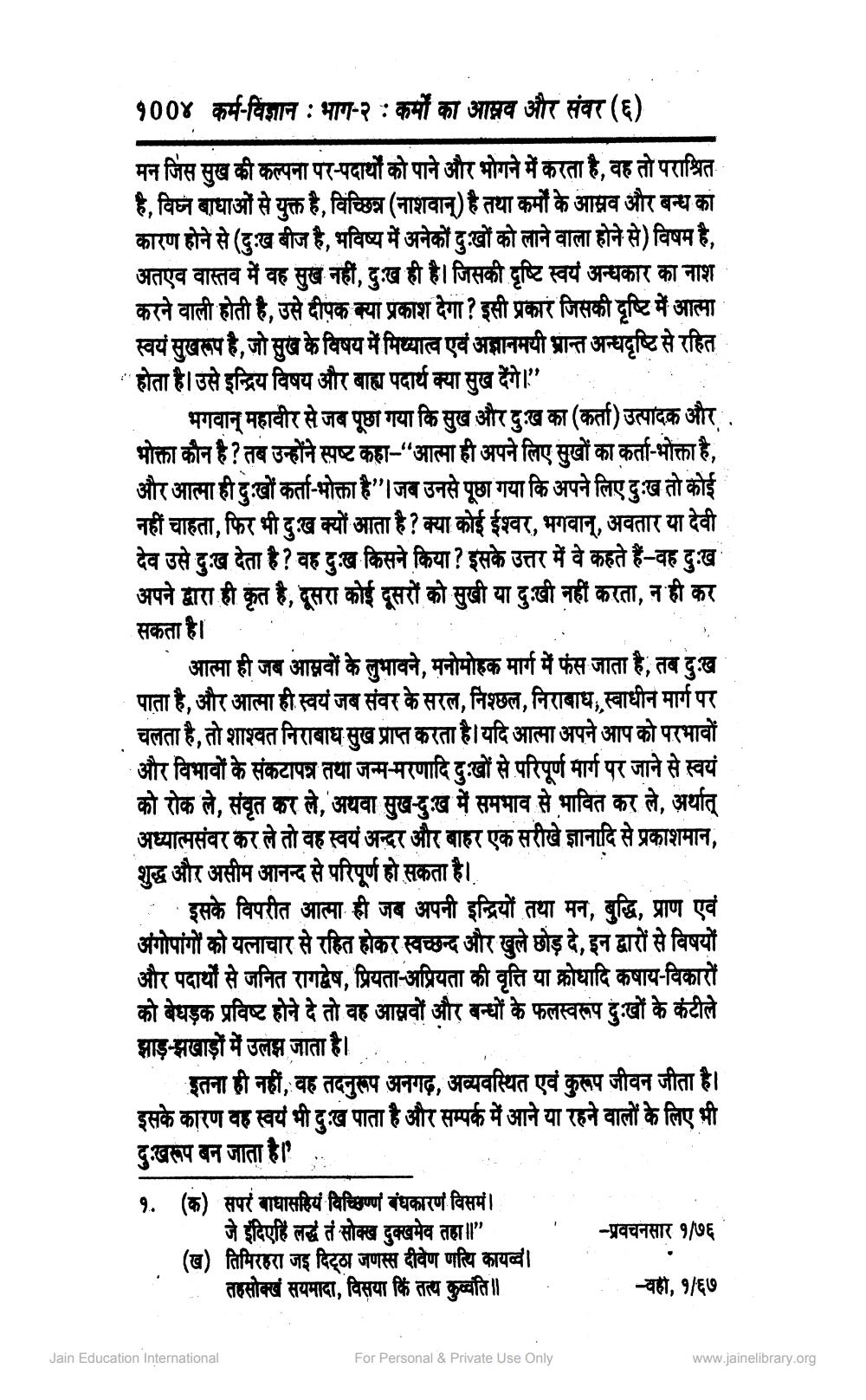________________
१००४ कर्म - विज्ञान : भाग-२ : कर्मों का आनव और संवर (६)
मन जिस सुख की कल्पना पर-पदार्थों को पाने और भोगने में करता है, वह तो पराश्रित है, विघ्न बाधाओं से युक्त है, विच्छिन्न (नाशवान्) है तथा कर्मों के आस्रव और बन्ध का कारण होने से (दुःख बीज है, भविष्य में अनेकों दुःखों को लाने वाला होने से ) विषम है, अतएव वास्तव में वह सुख नहीं, दुःख ही है। जिसकी दृष्टि स्वयं अन्धकार का नाश करने वाली होती है, उसे दीपक क्या प्रकाश देगा ? इसी प्रकार जिसकी दृष्टि में आत्मा स्वयं सुखरूप है, जो सुख के विषय में मिध्यात्व एवं अज्ञानमयी प्रान्त अन्धदृष्टि से रहित होता है। उसे इन्द्रिय विषय और बाह्य पदार्थ क्या सुख देंगे।"
भगवान् महावीर से जब पूछा गया कि सुख और दुःख का (कर्ता) उत्पादक और भोक्ता कौन है? तब उन्होंने स्पष्ट कहा - "आत्मा ही अपने लिए सुखों का कर्ता-भोक्ता है, और आत्मा ही दुःखकर्ता भोक्ता है"। जब उनसे पूछा गया कि अपने लिए दुःख तो कोई नहीं चाहता, फिर भी दुःख क्यों आता है ? क्या कोई ईश्वर, भगवान्, अवतार या देवी देव उसे दुःख देता है? वह दुःख किसने किया? इसके उत्तर में वे कहते हैं - वह दुःख अपने द्वारा ही कृत है, दूसरा कोई दूसरों को सुखी या दुःखी नहीं करता, न ही कर सकता है।
आत्मा ही जब आनवों के लुभावने, मनोमोहक मार्ग में फंस जाता है, तब दुःख पाता है, और आत्मा ही स्वयं जब संवर के सरल, निश्छल, निराबाध, स्वाधीन मार्ग पर चलता है, तो शाश्वत निराबाध सुख प्राप्त करता है। यदि आत्मा अपने आप को परभावों और विभावों के संकटापन्न तथा जन्म-मरणादि दुःखों से परिपूर्ण मार्ग पर जाने से स्वयं को रोक ले, संवृत कर ले, अथवा सुख-दुःख में समभाव से भावित कर ले, अर्थात् अध्यात्मसंवर कर ले तो वह स्वयं अन्दर और बाहर एक सरीखे ज्ञानादि से प्रकाशमान, शुद्ध और असीम आनन्द से परिपूर्ण हो सकता है।.
इसके विपरीत आत्मा ही जब अपनी इन्द्रियों तथा मन, बुद्धि, प्राण एवं अंगोपांगों को यनाचार से रहित होकर स्वच्छन्द और खुले छोड़ दे, इन द्वारों से विषयों और पदार्थों से जनित रागद्वेष, प्रियता- अप्रियता की वृत्ति या क्रोधादि कषाय-विकारों को बेधड़क प्रविष्ट होने दे तो वह आनवों और बन्धों के फलस्वरूप दुःखों के कंटीले झाड़-झखाड़ों में उलझ जाता है।
इतना ही नहीं, वह तदनुरूप अनगढ़, अव्यवस्थित एवं कुरूप जीवन जीता है। इसके कारण वह स्वयं भी दुःख पाता है और सम्पर्क में आने या रहने वालों के लिए भी दुःखरूप बन जाता है।'
9. (क) सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जे इदिएहिं लद्धं तं सोक्ख दुक्खमेव तहा ॥” (ख) तिमिरहरा जइ दिट्ठा जणस्स दीवेण णत्थि कायव्वं । तहसोक्खं सयमादा, विसया किं तत्य कुब्वति ॥
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
- प्रवचनसार १/७६
वही, १/६७
www.jainelibrary.org