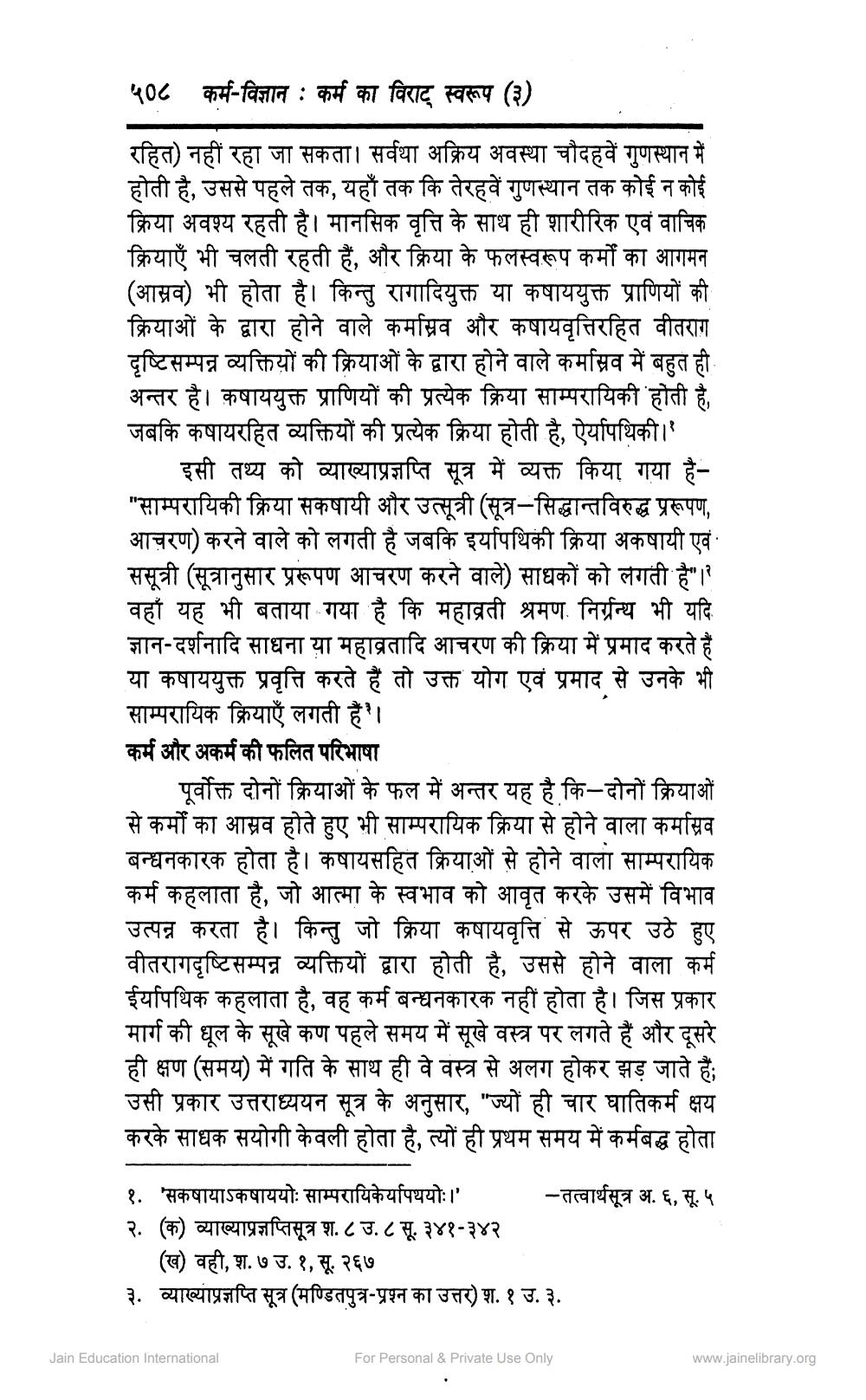________________
५०८
कर्म-विज्ञान : कर्म का विराट् स्वरूप (३)
रहित) नहीं रहा जा सकता। सर्वथा अक्रिय अवस्था चौदहवें गुणस्थान में होती है, उससे पहले तक, यहाँ तक कि तेरहवें गुणस्थान तक कोई न कोई क्रिया अवश्य रहती है। मानसिक वृत्ति के साथ ही शारीरिक एवं वाचिक क्रियाएँ भी चलती रहती हैं, और क्रिया के फलस्वरूप कर्मों का आगमन (आम्रव) भी होता है। किन्तु रागादियुक्त या कषाययुक्त प्राणियों की क्रियाओं के द्वारा होने वाले कर्मास्रव और कषायवृत्तिरहित वीतराग दृष्टिसम्पन्न व्यक्तियों की क्रियाओं के द्वारा होने वाले कर्मास्रव में बहुत ही अन्तर है। कषाययुक्त प्राणियों की प्रत्येक क्रिया साम्परायिकी होती है, जबकि कषायरहित व्यक्तियों की प्रत्येक क्रिया होती है, ऐपिथिकी।
इसी तथ्य को व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र में व्यक्त किया गया है"साम्परायिकी क्रिया सकषायी और उत्सूत्री (सूत्र-सिद्धान्तविरुद्ध प्ररूपण, आचरण) करने वाले को लगती है जबकि इर्यापथिकी क्रिया अकषायी एवं ससूत्री (सूत्रानुसार प्ररूपण आचरण करने वाले) साधकों को लगती है"।' वहाँ यह भी बताया गया है कि महाव्रती श्रमण निर्ग्रन्थ भी यदि ज्ञान-दर्शनादि साधना या महाव्रतादि आचरण की क्रिया में प्रमाद करते हैं या कषाययुक्त प्रवृत्ति करते हैं तो उक्त योग एवं प्रमाद से उनके भी साम्परायिक क्रियाएँ लगती हैं। कर्म और अकर्म की फलित परिभाषा
पूर्वोक्त दोनों क्रियाओं के फल में अन्तर यह है कि-दोनों क्रियाओं से कर्मों का आस्रव होते हुए भी साम्परायिक क्रिया से होने वाला कर्मास्रव बन्धनकारक होता है। कषायसहित क्रियाओं से होने वाला साम्परायिक कर्म कहलाता है, जो आत्मा के स्वभाव को आवृत करके उसमें विभाव उत्पन्न करता है। किन्तु जो क्रिया कषायवृत्ति से ऊपर उठे हुए वीतरागदृष्टिसम्पन्न व्यक्तियों द्वारा होती है, उससे होने वाला कर्म ईर्यापथिक कहलाता है, वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता है। जिस प्रकार मार्ग की धूल के सूखे कण पहले समय में सूखे वस्त्र पर लगते हैं और दूसरे ही क्षण (समय) में गति के साथ ही वे वस्त्र से अलग होकर झड़ जाते हैं; उसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार, "ज्यों ही चार घातिकर्म क्षय करके साधक सयोगी केवली होता है, त्यों ही प्रथम समय में कर्मबद्ध होता १. 'सकषायाऽकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः।' -तत्वार्थसूत्र अ. ६, सू. ५ २. (क) व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र श. ८ उ. ८ सू. ३४१-३४२
(ख) वही, श. ७ उ. १, सू. २६७ ३. व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र (मण्डितपुत्र-प्रश्न का उत्तर) श. १ उ. ३.
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org