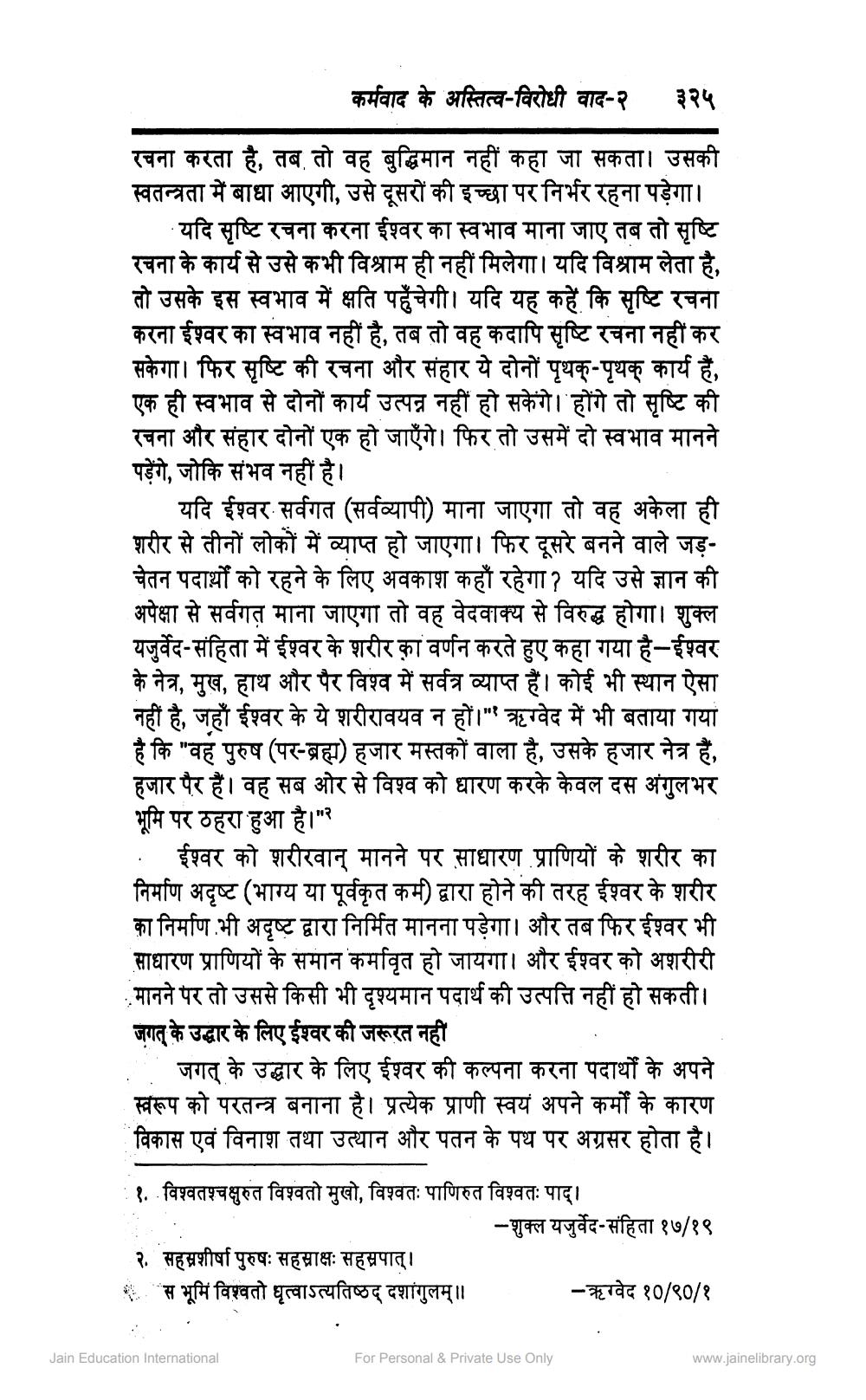________________
कर्मवाद के अस्तित्व-विरोधी वाद-२
३२५
रचना करता है, तब तो वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। उसकी स्वतन्त्रता में बाधा आएगी, उसे दूसरों की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ेगा। __ यदि सृष्टि रचना करना ईश्वर का स्वभाव माना जाए तब तो सृष्टि रचना के कार्य से उसे कभी विश्राम ही नहीं मिलेगा। यदि विश्राम लेता है, तो उसके इस स्वभाव में क्षति पहुँचेगी। यदि यह कहें कि सष्टि रचना करना ईश्वर का स्वभाव नहीं है, तब तो वह कदापि सृष्टि रचना नहीं कर सकेगा। फिर सृष्टि की रचना और संहार ये दोनों पृथक्-पृथक् कार्य हैं, एक ही स्वभाव से दोनों कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। होंगे तो सृष्टि की रचना और संहार दोनों एक हो जाएँगे। फिर तो उसमें दो स्वभाव मानने पड़ेंगे, जोकि संभव नहीं है।
यदि ईश्वर सर्वगत (सर्वव्यापी) माना जाएगा तो वह अकेला ही शरीर से तीनों लोकों में व्याप्त हो जाएगा। फिर दूसरे बनने वाले जड़चेतन पदार्थों को रहने के लिए अवकाश कहाँ रहेगा? यदि उसे ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत माना जाएगा तो वह वेदवाक्य से विरुद्ध होगा। शुक्ल यजुर्वेद-संहिता में ईश्वर के शरीर का वर्णन करते हुए कहा गया है-ईश्वर के नेत्र, मुख, हाथ और पैर विश्व में सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ ईश्वर के ये शरीरावयव न हों।" ऋग्वेद में भी बताया गया है कि "वह पुरुष (पर-ब्रह्म) हजार मस्तकों वाला है, उसके हजार नेत्र हैं, हजार पैर है। वह सब ओर से विश्व को धारण करके केवल दस अंगुलभर भूमि पर ठहरा हुआ है।"२ . ईश्वर को शरीरवान् मानने पर साधारण प्राणियों के शरीर का निर्माण अदृष्ट (भाग्य या पूर्वकृत कम) द्वारा होने की तरह ईश्वर के शरीर का निर्माण भी अदृष्ट द्वारा निर्मित मानना पड़ेगा। और तब फिर ईश्वर भी साधारण प्राणियों के समान कर्मावृत हो जायगा। और ईश्वर को अशरीरी मानने पर तो उससे किसी भी दृश्यमान पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जगत् के उद्धार के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं
जगत् के उद्धार के लिए ईश्वर की कल्पना करना पदार्थों के अपने स्वरूप को परतन्त्र बनाना है। प्रत्येक प्राणी स्वयं अपने कर्मों के कारण विकास एवं विनाश तथा उत्थान और पतन के पथ पर अग्रसर होता है।
१. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतः पाणिरुत विश्वतः पाद्।
-शुक्ल यजुर्वेद-संहिता १७/१९ २. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमि विश्वतो धृत्वाऽत्यतिष्ठद् दशांगुलम्॥ -ऋग्वेद १०/९०/१
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org