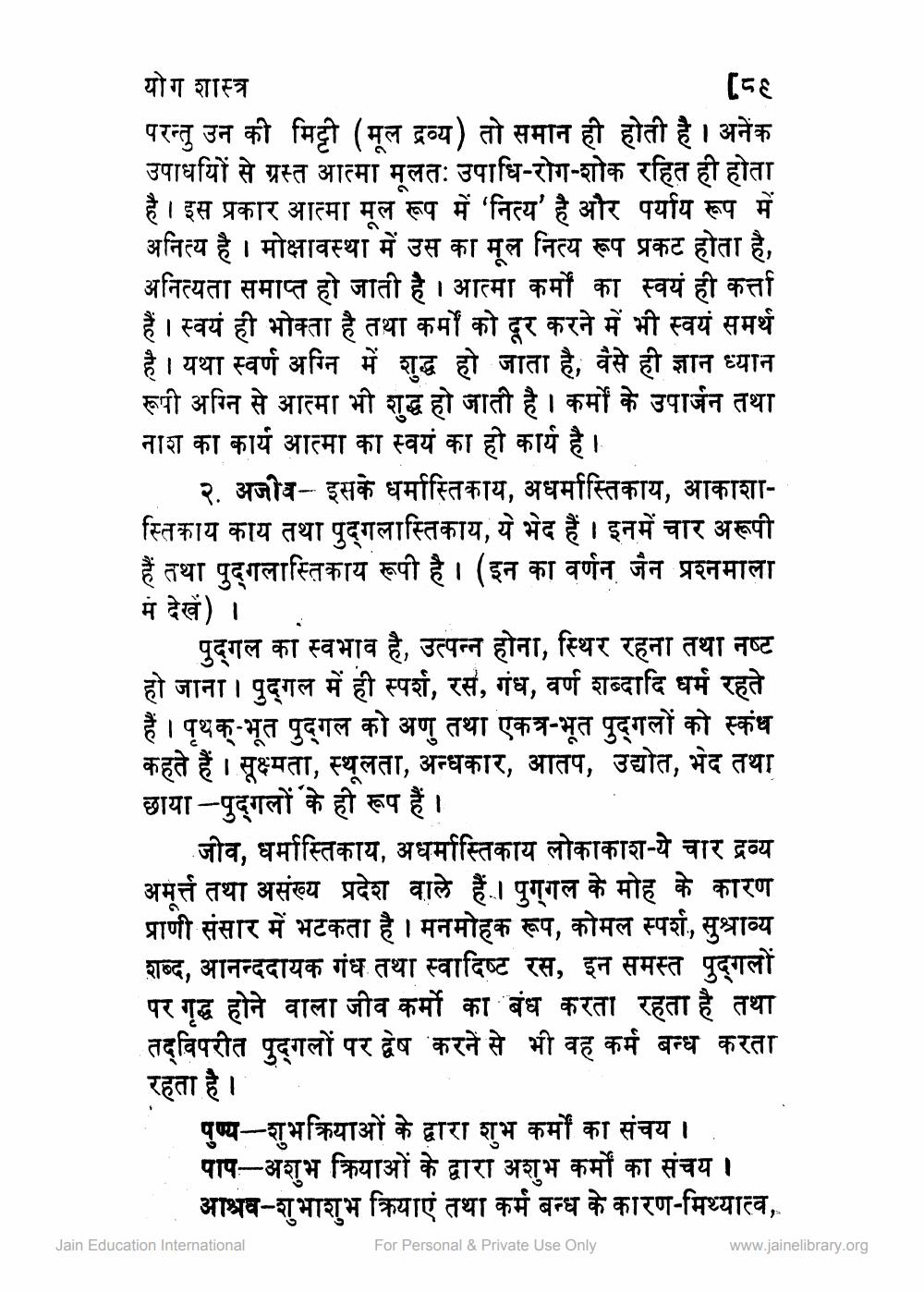________________
योग शास्त्र
[८६ परन्तु उन की मिट्टी (मूल द्रव्य) तो समान ही होती है । अनेक उपाधयिों से ग्रस्त आत्मा मूलतः उपाधि-रोग-शोक रहित ही होता है । इस प्रकार आत्मा मूल रूप में 'नित्य' है और पर्याय रूप में अनित्य है । मोक्षावस्था में उस का मूल नित्य रूप प्रकट होता है, अनित्यता समाप्त हो जाती है। आत्मा कर्मों का स्वयं ही कर्ता हैं । स्वयं ही भोक्ता है तथा कर्मों को दूर करने में भी स्वयं समर्थ है। यथा स्वर्ण अग्नि में शद्ध हो जाता है, वैसे ही ज्ञान ध्यान रूपी अग्नि से आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। कर्मों के उपार्जन तथा नाश का कार्य आत्मा का स्वयं का हो कार्य है।
२. अजीव- इसके धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय काय तथा पुद्गलास्तिकाय, ये भेद हैं । इनमें चार अरूपी हैं तथा पुद्गलास्तिकाय रूपी है । (इन का वर्णन जैन प्रश्नमाला म देखें)।
पुद्गल का स्वभाव है, उत्पन्न होना, स्थिर रहना तथा नष्ट हो जाना। पुद्गल में ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दादि धर्म रहते हैं । पृथक्-भूत पुद्गल को अणु तथा एकत्र-भूत पुद्गलों को स्कंध कहते हैं । सूक्ष्मता, स्थूलता, अन्धकार, आतप, उद्योत, भेद तथा छाया-पुद्गलों के ही रूप हैं। ___ जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय लोकाकाश-ये चार द्रव्य अमूर्त तथा असंख्य प्रदेश वाले हैं। पुग्गल के मोह के कारण प्राणी संसार में भटकता है । मनमोहक रूप, कोमल स्पर्श, सुश्राव्य शब्द, आनन्ददायक गंध तथा स्वादिष्ट रस, इन समस्त पुद्गलों पर गद्ध होने वाला जीव कर्मों का बंध करता रहता है तथा तद्विपरीत पुद्गलों पर द्वेष करने से भी वह कर्म बन्ध करता रहता है।
पुण्य-शुभक्रियाओं के द्वारा शुभ कर्मों का संचय । पाप-अशुभ क्रियाओं के द्वारा अशुभ कर्मों का संचय । आश्रध-शुभाशुभ क्रियाएं तथा कर्म बन्ध के कारण-मिथ्यात्व,
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org