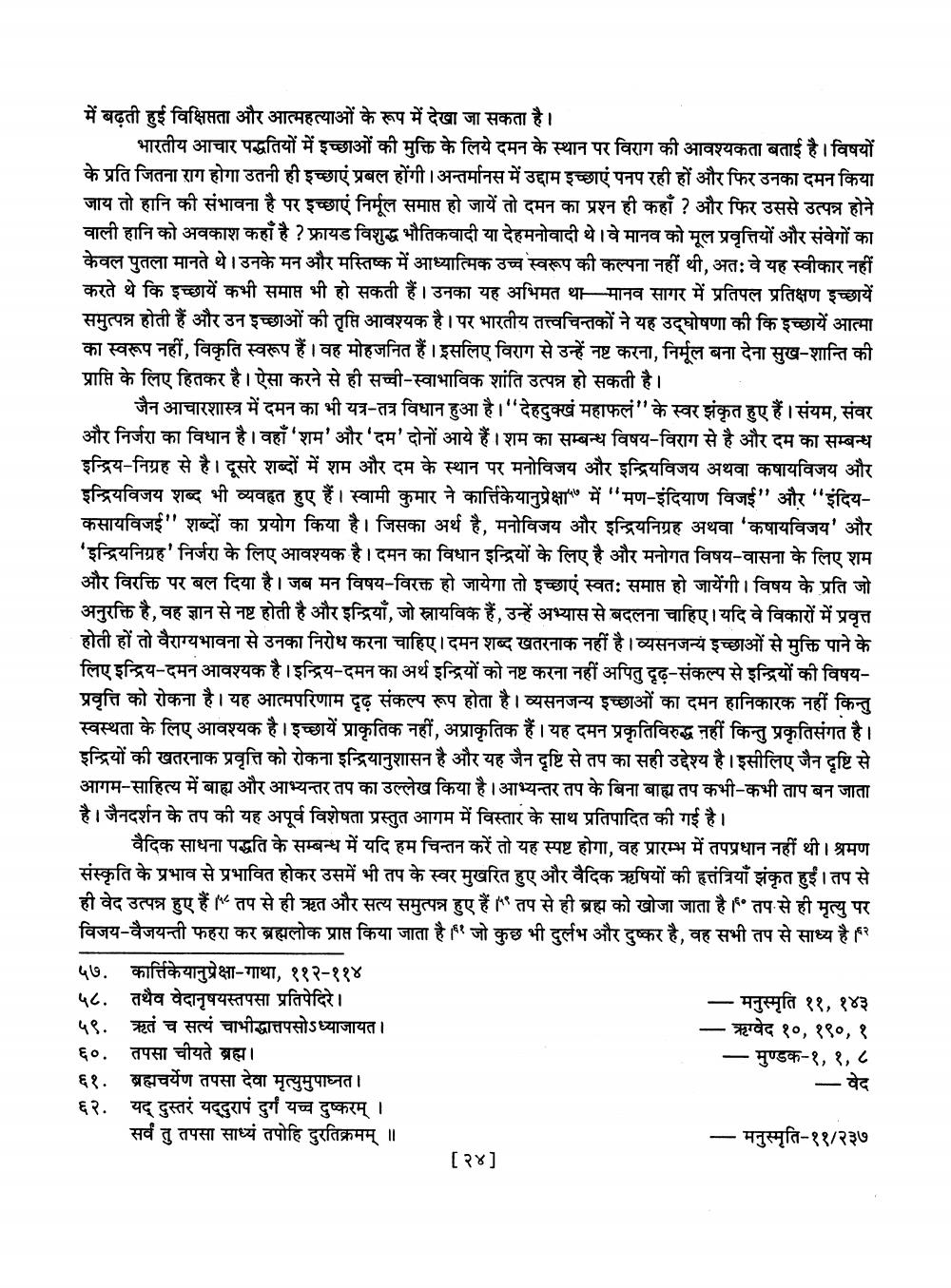________________
और निर्जरा का वि
में बढ़ती हुई विक्षिप्तता और आत्महत्याओं के रूप में देखा जा सकता है।
भारतीय आचार पद्धतियों में इच्छाओं की मुक्ति के लिये दमन के स्थान पर विराग की आवश्यकता बताई है। विषयों के प्रति जितना राग होगा उतनी ही इच्छाएं प्रबल होंगी।अन्तर्मानस में उद्दाम इच्छाएं पनप रही हों और फिर उनका दमन किया जाय तो हानि की संभावना है पर इच्छाएं निर्मल समाप्त हो जायें तो दमन का प्रश्न ही कहाँ? और फिर उससे उत्पन्न होने वाली हानि को अवकाश कहाँ है ? फ्रायड विशुद्ध भौतिकवादी या देहमनोवादी थे। वे मानव को मूल प्रवृत्तियों और संवेगों का केवल पुतला मानते थे। उनके मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक उच्च स्वरूप की कल्पना नहीं थी, अत: वे यह स्वीकार नहीं करते थे कि इच्छायें कभी समाप्त भी हो सकती हैं। उनका यह अभिमत था-मानव सागर में प्रतिपल प्रतिक्षण इच्छायें समुत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं की तृप्ति आवश्यक है। पर भारतीय तत्त्वचिन्तकों ने यह उद्घोषणा की कि इच्छायें आत्मा का स्वरूप नहीं, विकृति स्वरूप हैं । वह मोहजनित हैं। इसलिए विराग से उन्हें नष्ट करना, निर्मूल बना देना सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिए हितकर है। ऐसा करने से ही सच्ची-स्वाभाविक शांति उत्पन्न हो सकती है।
जैन आचारशास्त्र में दमन का भी यत्र-तत्र विधान हुआ है।"देहदुक्खं महाफलं"के स्वर झंकृत हुए हैं। संयम, संवर नर्जरा का विधान है। वहाँ 'शम' और 'दम' दोनों आये हैं। शम का सम्बन्ध विषय-विराग से है और दम का सम्बन्ध इन्द्रिय-निग्रह से है। दूसरे शब्दों में शम और दम के स्थान पर मनोविजय और इन्द्रियविजय अथवा कषायविजय और इन्द्रियविजय शब्द भी व्यवहृत हुए हैं। स्वामी कुमार ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा" में "मण-इंदियाण विजई" और "इंदियकसायविजई" शब्दों का प्रयोग किया है। जिसका अर्थ है, मनोविजय और इन्द्रियनिग्रह अथवा 'कषायविजय' और 'इन्द्रियनिग्रह' निर्जरा के लिए आवश्यक है। दमन का विधान इन्द्रियों के लिए है और मनोगत विषय-वासना के लिए शम
और विरक्ति पर बल दिया है। जब मन विषय-विरक्त हो जायेगा तो इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी। विषय के प्रति जो अनुरक्ति है, वह ज्ञान से नष्ट होती है और इन्द्रियाँ, जो स्नायविक हैं, उन्हें अभ्यास से बदलना चाहिए। यदि वे विकारों में प्रवृत्त होती हों तो वैराग्यभावना से उनका निरोध करना चाहिए। दमन शब्द खतरनाक नहीं है। व्यसनजन्य इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए इन्द्रिय-दमन आवश्यक है। इन्द्रिय-दमन का अर्थ इन्द्रियों को नष्ट करना नहीं अपितु दृढ़-संकल्प से इन्द्रियों की विषयप्रवृत्ति को रोकना है। यह आत्मपरिणाम दृढ़ संकल्प रूप होता है। व्यसनजन्य इच्छाओं का दमन हानिकारक नहीं किन्तु स्वस्थता के लिए आवश्यक है। इच्छायें प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक हैं । यह दमन प्रकृतिविरुद्ध नहीं किन्तु प्रकृतिसंगत है। इन्द्रियों की खतरनाक प्रवृत्ति को रोकना इन्द्रियानुशासन है और यह जैन दृष्टि से तप का सही उद्देश्य है। इसीलिए जैन दृष्टि से आगम-साहित्य में बाह्य और आभ्यन्तर तप का उल्लेख किया है। आभ्यन्तर तप के बिना बाह्य तप कभी-कभी ताप बन जाता है। जैनदर्शन के तप की यह अपूर्व विशेषता प्रस्तुत आगम में विस्तार के साथ प्रतिपादित की गई है।
___वैदिक साधना पद्धति के सम्बन्ध में यदि हम चिन्तन करें तो यह स्पष्ट होगा, वह प्रारम्भ में तपप्रधान नहीं थी। श्रमण संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित होकर उसमें भी तप के स्वर मुखरित हुए और वैदिक ऋषियों की हृत्तंत्रियों झंकृत ही वेद उत्पन्न हए हैं तप से ही ऋत और सत्य समत्पन्न हुए हैं। तप से ही ब्रह्म को खोजा जाता है। तप से ही मृत्यु पर विजय-वैजयन्ती फहरा कर ब्रह्मलोक प्राप्त किया जाता है। जो कुछ भी दुर्लभ और दुष्कर है, वह सभी तप से साध्य है।६२
५७. कार्तिकेयानुप्रेक्षा-गाथा, ११२-११४ ५८. तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे। ५९. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्याजायत। ६०. तपसा चीयते ब्रह्म। ६१. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत । ६२. यद् दुस्तरं यदुरापं दुर्गं यच्च दुष्करम् ।
सर्वं तु तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम् ॥
मनुस्मृति ११, १४३ - ऋग्वेद १०, १९०, १
-मुण्डक-१, १,८
-वेद
- मनुस्मृति-११/२३७
[२४]