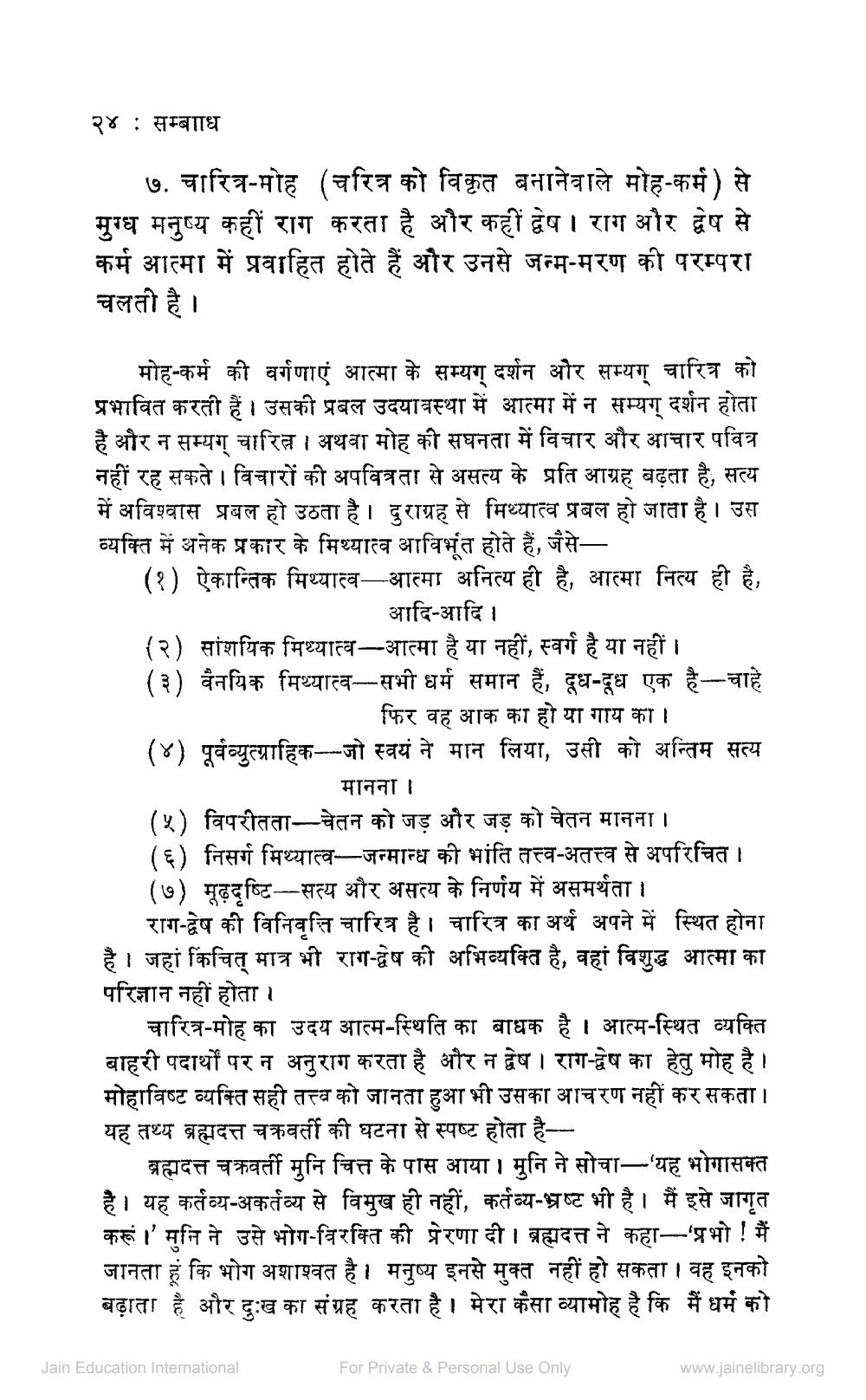________________
२४ : सम्बाध
७. चारित्र-मोह (चरित्र को विकृत बनानेवाले मोह-कर्म) से मुग्ध मनुष्य कहीं राग करता है और कहीं द्वेष । राग और द्वेष से कर्म आत्मा में प्रवाहित होते हैं और उनसे जन्म-मरण की परम्परा चलती है।
मोह-कर्म की वर्गणाएं आत्मा के सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र को प्रभावित करती हैं। उसकी प्रबल उदयावस्था में आत्मा में न सम्यग् दर्शन होता है और न सम्यग् चारित्र । अथवा मोह की सघनता में विचार और आचार पवित्र नहीं रह सकते। विचारों की अपवित्रता से असत्य के प्रति आग्रह बढ़ता है, सत्य में अविश्वास प्रबल हो उठता है। दुराग्रह से मिथ्यात्व प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति में अनेक प्रकार के मिथ्यात्व आविर्भूत होते हैं, जैसे(१) ऐकान्तिक मिथ्यात्व-आत्मा अनित्य ही है, आत्मा नित्य ही है,
आदि-आदि। (२) सांशयिक मिथ्यात्व-आत्मा है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं। (३) वैनयिक मिथ्यात्व-सभी धर्म समान हैं, दूध-दूध एक है-चाहे
फिर वह आक का हो या गाय का। (४) पूर्वव्युत्प्राहिक-जो स्वयं ने मान लिया, उसी को अन्तिम सत्य
__ मानना। (५) विपरीतता-चेतन को जड़ और जड़ को चेतन मानना। (६) निसर्ग मिथ्यात्व-जन्मान्ध की भांति तत्त्व-अतत्त्व से अपरिचित । (७) मूढ़दृष्टि-सत्य और असत्य के निर्णय में असमर्थता।
राग-द्वेष की विनिवृत्ति चारित्र है। चारित्र का अर्थ अपने में स्थित होना है। जहां किंचित् मात्र भी राग-द्वेष की अभिव्यक्ति है, वहां विशुद्ध आत्मा का परिज्ञान नहीं होता। __ चारित्र-मोह का उदय आत्म-स्थिति का बाधक है । आत्म-स्थित व्यक्ति बाहरी पदार्थों पर न अनुराग करता है और न द्वेष । राग-द्वेष का हेतु मोह है। मोहाविष्ट व्यक्ति सही तत्त्व को जानता हुआ भी उसका आचरण नहीं कर सकता। यह तथ्य ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की घटना से स्पष्ट होता है___ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मुनि चित्त के पास आया। मुनि ने सोचा-'यह भोगासक्त है। यह कर्तव्य-अकर्तव्य से विमुख ही नहीं, कर्तव्य-भ्रष्ट भी है। मैं इसे जागृत करूं ।' मुनि ने उसे भोग-विरक्ति की प्रेरणा दी। ब्रह्मदत्त ने कहा-'प्रभो ! मैं जानता हूं कि भोग अशाश्वत है। मनुष्य इनसे मुक्त नहीं हो सकता। वह इनको बढ़ाता है और दुःख का संग्रह करता है। मेरा कैसा व्यामोह है कि मैं धर्म को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org