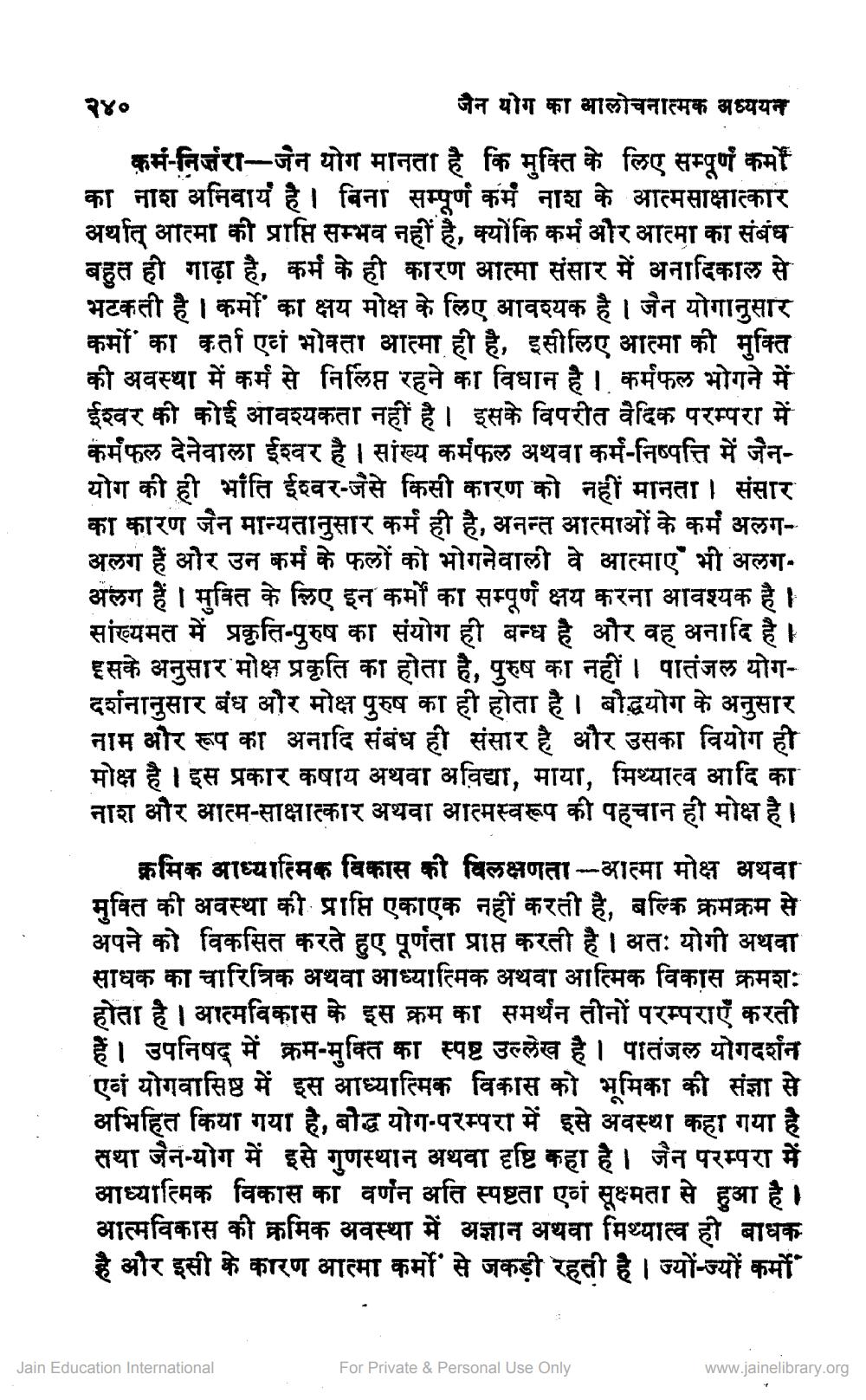________________
जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन
कर्म - निर्जरा - जैन योग मानता है कि मुक्ति के लिए सम्पूर्ण कर्मों का नाश अनिवार्य है । बिना सम्पूर्ण कर्म नाश के आत्मसाक्षात्कार अर्थात् आत्मा की प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि कर्म और आत्मा का संबंध बहुत ही गाढ़ा है, कर्म के ही कारण आत्मा संसार में अनादिकाल से भटकती है । कर्मों का क्षय मोक्ष के लिए आवश्यक है । जैन योगानुसार कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता आत्मा ही है, इसीलिए आत्मा की मुक्ति की अवस्था में कर्म से निर्लिप्त रहने का विधान है । कर्मफल भोगने में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत वैदिक परम्परा में कर्म फल देनेवाला ईश्वर है । सांख्य कर्मफल अथवा कर्म - निष्पत्ति में जैनयोग की ही भाँति ईश्वर-जैसे किसी कारण को नहीं मानता। संसार का कारण जैन मान्यतानुसार कर्म ही है, अनन्त आत्माओं के कर्म अलगअलग हैं और उन कर्म के फलों को भोगनेवाली वे आत्माएँ भी अलगअलग हैं । मुक्ति के लिए इन कर्मों का सम्पूर्ण क्षय करना आवश्यक है । सांख्यमत में प्रकृति - पुरुष का संयोग ही बन्ध है और वह अनादि है । इसके अनुसार मोक्ष प्रकृति का होता है, पुरुष का नहीं । पातंजल योगदर्शनानुसार बंध और मोक्ष पुरुष का ही होता है । बौद्धयोग के अनुसार नाम और रूप का अनादि संबंध ही संसार है और उसका वियोग ही मोक्ष है । इस प्रकार कषाय अथवा अविद्या, माया, मिथ्यात्व आदि का नाश और आत्म-साक्षात्कार अथवा आत्मस्वरूप की पहचान ही मोक्ष है ।
२४०
क्रमिक आध्यात्मिक विकास की विलक्षणता - आत्मा मोक्ष अथवा मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति एकाएक नहीं करती है, बल्कि क्रमक्रम से अपने को विकसित करते हुए पूर्णता प्राप्त करती है । अतः योगी अथवा साधक का चारित्रिक अथवा आध्यात्मिक अथवा आत्मिक विकास क्रमशः होता है । आत्मविकास के इस क्रम का समर्थन तीनों परम्पराएँ करती हैं । उपनिषद् में क्रम - मुक्ति का स्पष्ट उल्लेख है । पातंजल योगदर्शन एवं योगवासिष्ठ में इस आध्यात्मिक विकास को भूमिका की संज्ञा से अभिहित किया गया है, बोद्ध योग परम्परा में इसे अवस्था कहा गया है तथा जैन- योग में इसे गुणस्थान अथवा दृष्टि कहा है। जैन परम्परा में आध्यात्मिक विकास का वर्णन अति स्पष्टता एवं सूक्ष्मता से हुआ है । आत्मविकास की क्रमिक अवस्था में अज्ञान अथवा मिथ्यात्व हो बाधक है और इसी के कारण आत्मा कर्मों से जकड़ी रहती है। ज्यों-ज्यों कर्मों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org