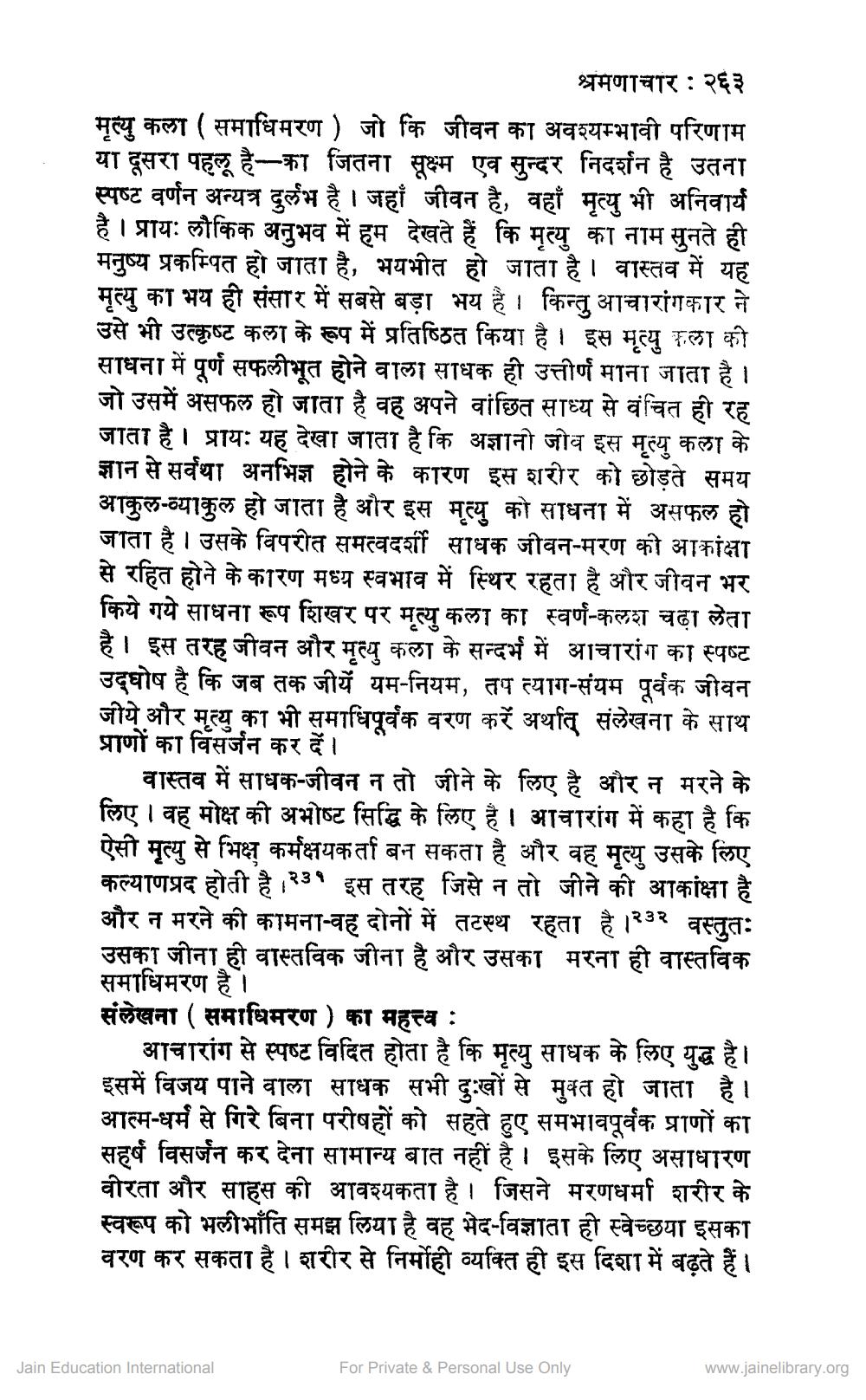________________
श्रमणाचार : २६३ मृत्यु कला (समाधिमरण ) जो कि जीवन का अवश्यम्भावी परिणाम या दूसरा पहलू है—का जितना सूक्ष्म एव सुन्दर निदर्शन है उतना स्पष्ट वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है । जहाँ जीवन है, वहाँ मृत्यु भी अनिवार्य है । प्रायः लौकिक अनुभव में हम देखते हैं कि मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य प्रकम्पित हो जाता है, भयभीत हो जाता है । वास्तव में यह मृत्यु का भय ही संसार में सबसे बड़ा भय है । किन्तु आचारांगकार ने उसे भी उत्कृष्ट कला के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इस मृत्यु कला की साधना में पूर्ण सफलीभूत होने वाला साधक ही उत्तीर्ण माना जाता है । जो उसमें असफल हो जाता है वह अपने वांछित साध्य से वंचित ही रह जाता है । प्रायः यह देखा जाता है कि अज्ञानी जीव इस मृत्यु कला के ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ होने के कारण इस शरीर को छोड़ते समय आकुल-व्याकुल हो जाता है और इस मृत्यु को साधना में असफल हो जाता है । उसके विपरीत समत्वदर्शी साधक जीवन-मरण की आकांक्षा से रहित होने के कारण मध्य स्वभाव में स्थिर रहता है और जीवन भर किये गये साधना रूप शिखर पर मृत्यु कला का स्वर्ण कलश चढ़ा लेता है । इस तरह जीवन और मृत्यु कला के सन्दर्भ में आचारांग का स्पष्ट उद्घोष है कि जब तक जीयें यम-नियम, तप त्याग-संयम पूर्वक जीवन जये और मृत्यु का भी समाधिपूर्वक वरण करें अर्थात् संलेखना के साथ प्राणों का विसर्जन कर दें ।
वास्तव में साधक - जीवन न तो जीने के लिए है और न मरने के लिए । वह मोक्ष की अभोष्ट सिद्धि के लिए है । आचारांग में कहा है कि ऐसी मृत्यु से भिक्षु कर्मक्षयकर्ता बन सकता है और वह मृत्यु उसके लिए कल्याणप्रद होती है । २३१ इस तरह जिसे न तो जीने की आकांक्षा है और न मरने की कामना - वह दोनों में तटस्थ रहता है | २३२ वस्तुतः उसका जीना ही वास्तविक जीना है और उसका मरना ही वास्तविक समाधिमरण है ।
संलेखना ( समाधिमरण ) का महत्त्व :
आचारांग से स्पष्ट विदित होता है कि मृत्यु साधक के लिए युद्ध है। इसमें विजय पाने वाला साधक सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है। आत्म-धर्म से गिरे बिना परीषहों को सहते हुए समभावपूर्वक प्राणों का सहर्षं विसर्जन कर देना सामान्य बात नहीं है । इसके लिए असाधारण वीरता और साहस की आवश्यकता है। जिसने मरणधर्मा शरीर के स्वरूप को भलीभाँति समझ लिया है वह भेद विज्ञाता ही स्वेच्छया इसका वरण कर सकता है । शरीर से निर्मोही व्यक्ति ही इस दिशा में बढ़ते हैं ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org